HI/BG 5.3
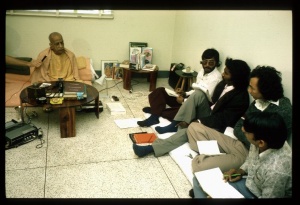
श्लोक 3
- ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।
- निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥३॥
शब्दार्थ
ज्ञेय:—जानना चाहिए; स:—वह; नित्य—सदैव; सन्न्यासी—संन्यासी; य:—जो; न—कभी नहीं; द्वेष्टि—घृणा करता है; न—न तो; काङ्क्षति—इच्छा करता है; निद्र्वन्द्व:—समस्त द्वैतताओं से मुक्त; हि—निश्चय ही; महा-बाहो—हे बलिष्ठ भुजाओं वाले; सुखम्—सुखपूर्वक; बन्धात्—बन्धन से; प्रमुच्यते—पूर्णतया मुक्त हो जाता है।
अनुवाद
जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य संन्यासी जाना जाता है | हे महाबाहु अर्जुन! ऐसा मनुष्य समस्त द्वन्द्वों से रहित होकर भवबन्धन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है |
तात्पर्य
पूर्णतया कृष्णभावनाभावित पुरुष नित्य संन्यासी है क्योंकि वह अपने कर्मफल से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांशा करता है | ऐसा संन्यासी, भगवान् की दिव्य प्रेमभक्ति के परायण होकर पूर्णज्ञानी होता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है | वह भलीभाँति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण (अंशी) है और वह स्वयं अंशमात्र है | ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है | कृष्ण-तादात्मय की भावना भ्रान्त है क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता | यह ज्ञान कि एकता गुणों की है न कि गुणों की मात्रा की, सही दिव्यज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिससे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न किसी का शोक | उसके मन में किसी प्रकार का छल-कपट नहीं रहता क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है | इस प्रकार छल-कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत् से भी मुक्त हो जाता है |