HI/BG 3.6
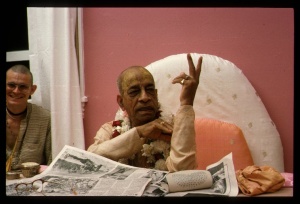
श्लोक 6
- कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।
- इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते ॥ ६॥
शब्दार्थ
कर्म-इन्द्रियाणि—पाँचों कर्मेन्द्रियों को; संयम्य—वश में करके; य:—जो; आस्ते—रहता है; मनसा—मन से; स्मरन्—सोचता हुआ; इन्द्रिय-अर्थान्—इन्द्रियविषयों को; विमूढ—मूर्ख; आत्मा—जीव; मिथ्या-आचार:—दम्भी; स:—वह; उच्यते—कहलाता है।
अनुवाद
जो कर्मेन्द्रियों को वश में तो करता है, किन्तु जिसका मन इन्द्रियविषयों का चिन्तन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है |
तात्पर्य
ऐसे अनेक मित्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्णभावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किन्तु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वात्सव में वे मन में इन्द्रियभोग का चिन्तन करते रहते हैं | ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों के बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किन्तु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं | इन्द्रियसुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है , किन्तु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधिविधानों के पालन में लिया जाय तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है | किन्तु जो अपने को योगी बताते हुए इन्द्रियतृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी-कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे | उसका ज्ञान व्यर्थ है क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान् की माया द्वारा हर लिये जाते हैं | ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता |